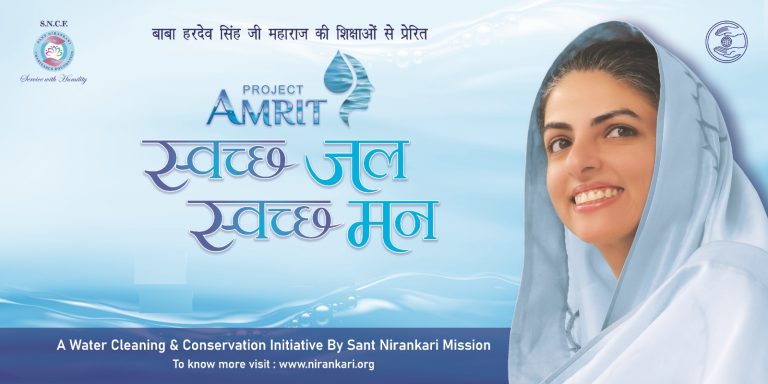■ सूर्यकांत उपाध्याय

महाभारत के उस मार्मिक क्षण में, जब युद्ध की विभीषिका सामने खड़ी थी, कर्ण ने श्रीकृष्ण से अपने हृदय का सारा विषाद उँडेल दिया। उसके स्वर में पीड़ा थी, आक्रोश था और कहीं न कहीं एक मौन प्रश्न भी।
कर्ण ने कहा- द्रोणाचार्य ने मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम ने विद्या दी, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि निर्णायक क्षण में मुझे वह विद्या स्मरण नहीं रहेगी। एक निरपराध गाय पर संयोगवश बाण लग गया तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्रापित कर दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। माता कुंती ने भी जन्म-रहस्य तब बताया, जब उन्हें अपने अन्य पुत्रों की चिंता थी। जो कुछ सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थान मुझे मिला, वह दुर्योधन के कारण मिला। यदि मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ, तो क्या मेरा अपराध है?
श्रीकृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा- कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा पीछा कर रही थी। उसी रात माता-पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन शस्त्रों की ध्वनि में बीता; मेरा गौशाला में। तुमने राजसी शिक्षा पाई; मैंने तिरस्कार सहा। तुम्हें अपनी पसंद से विवाह का अधिकार मिला; मुझे नहीं। मुझे अपने कुल और प्रजा की रक्षा हेतु समुद्र तट पर नई नगरी बसानी पड़ी और रणछोड़ तक कहा गया।
फिर भी, प्रश्न यह नहीं कि किसे कितना कष्ट मिला। जीवन किसी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय सहा है तो युधिष्ठिर ने भी। किंतु सत्य और धर्म क्या है, यह तुम जानते हो।
कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा- अपमान, अभाव और पीड़ा हमें अधर्म का अधिकार नहीं देते। मनुष्य की पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके चुनावों से होती है। तुम वीर हो, दानी हो, परंतु धर्म की सीमा लांघकर वीरता भी कलंकित हो जाती है।
कर्ण मौन हो गया। उसे समझ आ रहा था कि उसका संघर्ष बाहरी शत्रुओं से अधिक अपने अंतर्मन से है। यह संवाद केवल दो महायोद्धाओं का नहीं था- यह धर्म और मोह, कर्तव्य और कृतज्ञता, सत्य और संबंधों के बीच चलने वाला शाश्वत संघर्ष था।