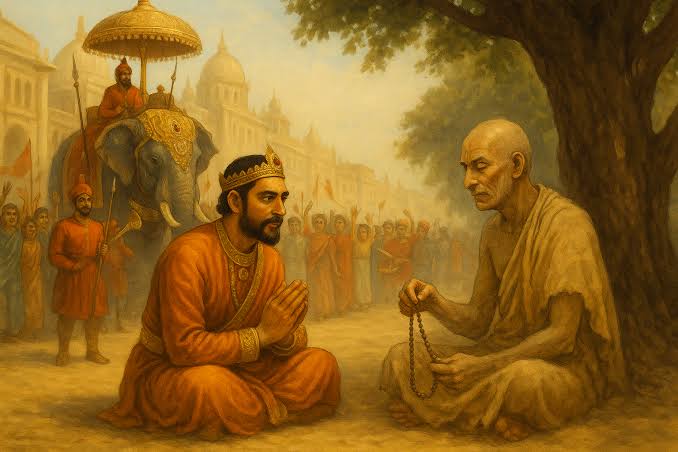■ सूर्यकांत उपाध्याय

वह रोज की तरह अपनी किराने की दुकान बंद कर ही रहे थे कि पीछे से एक मासूम आवाज़ आई “अंकल… अंकल…”
मुड़कर देखा तो सात-आठ साल की एक बच्ची हांफती हुई उनके पास आ रही थी।
उन्होंने पूछा, “क्या बात है, बेटा?”
बच्ची बोली, “अंकल, पंद्रह रुपए की कनियाँ और दस रुपए की दाल चाहिए थी।”
उन्होंने कहा, “दुकान बंद कर दी है, सुबह ले लेना।”
बच्ची बोली, “अभी चाहिए… घर में आटा भी नहीं है।”
उसकी बात सुनकर वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर ताले की चाबी निकालकर दुकान खोली और बिना तोले चावल-दाल थैले में डाल दी। बच्ची बोली, “धन्यवाद अंकल।”
उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “सावधानी से घर जाना।”
उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार-बार वही शब्द गूंजते रहे, “घर में आटा भी नहीं है।”
उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब पिता रिक्शा चलाते थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थीं और कई बार रोटी पानी में भिगोकर खानी पड़ती थी।
उन्होंने सोचा, “अब मेरे पास दुकान है, कमाई है… पर क्या मैंने इंसानियत भी कमाई?”
सुबह दुकान खोलते ही उन्होंने एक बोर्ड लगाया, “यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हों तो बेहिचक बताइए। सामान उधार नहीं, हक से मिलेगा।”
साथ ही एक डब्बा रखा, “जो मदद करना चाहे, इसमें पैसे डाल सकता है।”
धीरे-धीरे यह दुकान ‘इंसानियत वाली दुकान’ कहलाने लगी। बुज़ुर्ग, दिहाड़ी मजदूर और बच्चे यहां से इज्जत के साथ सामान लेते और जो समर्थ होते, वे डब्बे में कुछ न कुछ डालते जाते।
कई बच्चों ने अपनी गुल्लक तक से योगदान दिया।
एक दिन वही बच्ची फिर आई, “अंकल, पापा ने पैसे भेजे हैं, पिछली बार का जोड़ लीजिए।”
उन्होंने कहा, “बेटा, वो इंसानियत का कर्ज था, उसका कोई हिसाब नहीं होता।”
बच्ची मुस्कुराई, “पापा बोले हैं, अब से वे भी इस डब्बे में पैसे डालेंगे।”
यह सुनकर दुकानदार की आंखें भर आईं।
किसी ने ठीक कहा है, “नेकी कभी बेकार नहीं जाती।”
अब यह दुकान भरोसे और मानवता का प्रतीक बन चुकी थी।
लोग इसे देखने दूर-दूर से आने लगे, मीडिया ने खबर छापी “जहां मुनाफा नहीं, ज़रूरत की कीमत ज़्यादा है -पढ़िए भरोसे वाली दुकान की कहानी।”
आज भी उस दुकान के बाहर वही बोर्ड लगा है “यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हों, तो बेहिचक बताइए।”
और डब्बे में रोज कोई न कोई चुपचाप कुछ डाल जाता है।
एक बच्ची की मासूम ज़रूरत ने साबित कर दिया, “बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है।”