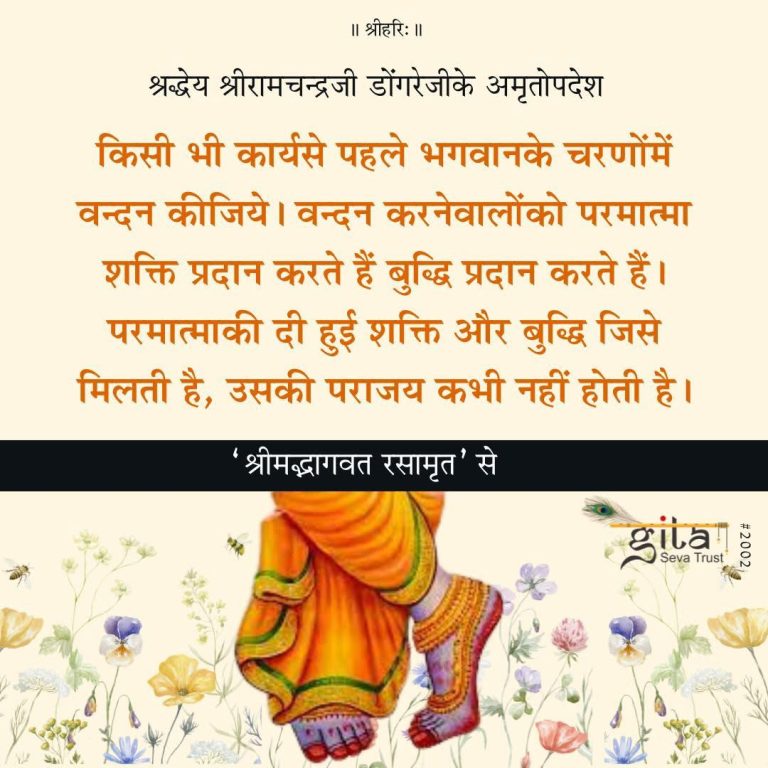■ सूर्यकांत उपाध्याय
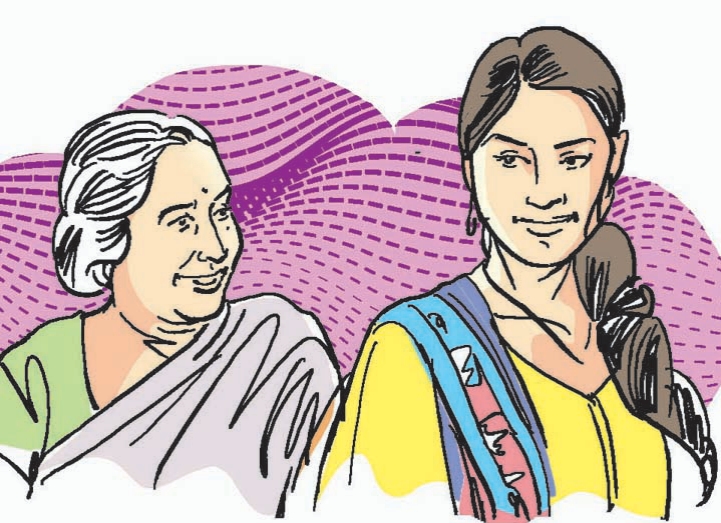
उस दिन के बाद घर की रसोई का दृश्य बदल गया।
सुबह सचमुच सुमन की फुर्ती से शुरू होती-चाय, नाश्ता, टिफ़िन, सब कुछ समय पर। मनोरमा जी पास बैठकर अख़बार पढ़तीं, पर बीच-बीच में कोई न कोई नुस्खा बता देतीं-“जीरा पहले भून लेना”, “दाल में ज़रा-सा हींग डालना मत भूलना।” सुमन ध्यान से सुनती, मानो कोई शिष्या अपने गुरु से विद्या ले रही हो।
शाम होते-होते रसोई का रंग बदल जाता। तब वह केवल भोजन बनाने की जगह नहीं रहती, वह अनुभव, स्मृतियों और स्नेह का आँगन बन जाती। मनोरमा जी पल्लू कमर में खोंसकर खड़ी होतीं और सुमन सचमुच उनकी सहायक बन जाती-सब्ज़ियाँ काटती, मसाले पकड़ाती, और बीच-बीच में पूछती, “माँ जी, इतना नमक ठीक है?”
धीरे-धीरे घर के बाकी सदस्य भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। ससुर जी हँसते हुए कहते, “अब तो हमारे घर में दो-दो रानियाँ हैं।” पति भी गर्व से दोस्तों से कहता, “मेरी पत्नी और माँ-दोनों के हाथ का स्वाद अलग है, पर प्यार एक-सा है।”
मनोरमा जी के चेहरे पर फिर वही आत्मविश्वास लौट आया। अब उन्हें ‘अदृश्य’ होने का भय नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि स्थान छिनता नहीं, बाँटा जाता है। और बाँटने से वह छोटा नहीं, बड़ा होता है।
एक शाम जब सुमन ने उनसे कहा, “माँ जी, आपके बिना यह घर अधूरा है,” तो मनोरमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया, “और तेरे बिना यह घर सूना।”
रसोई अब सत्ता का प्रतीक नहीं थी, संबंध का सेतु बन चुकी थी। वहाँ करछुल की खनक में अधिकार नहीं, अपनापन था; मसालों की खुशबू में प्रतिस्पर्धा नहीं, साझेदारी थी।
सुमन ने उस दिन एक बड़ा पाठ सीखा-
किसी का काम छीनकर सम्मान नहीं मिलता, सम्मान मिलता है किसी की पहचान को सहेजकर।
और मनोरमा जी ने भी समझ लिया-
नई पीढ़ी जगह लेने नहीं, साथ चलने आती है।
उस घर में अब हर शाम एक ही नाम गूँजता-
“रसोई की रानी”
पर सब जानते थे, वह एक नहीं, दो थीं।